समानता बनाम मनुवाद : यूजीसी नियमावली और जाति वर्चस्व का प्रतिरोध* *(आलेख : विक्रम सिंह)*
समानता बनाम मनुवाद : यूजीसी नियमावली और जाति वर्चस्व का प्रतिरोध*
*(आलेख : विक्रम सिंह)*

जे टी न्यूज
जाति प्रथा कितनी घृणित और अमानवीय है, यह हमारे देश में बताने की ज़रूरत नहीं है। दलितों पर रोज़ होने वाले अमानवीय अत्याचार और उनके साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार, इसकी चीख-चीख कर गवाही देते हैं। लेकिन जब जाति व्यवस्था को मनुवादी विचारधारा का राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, तो जाति व्यवस्था कितनी उग्र, आक्रामक और खुले रूप में सामने आती है, यह हमने पिछले कुछ हफ़्तों में साफ़ तौर पर देखा है।
जनवरी महीने में मीडिया और सोशल मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा था, जैसे देश में कोई बहुत बड़ा सामाजिक संकट आ गया हो। पूरे देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के संवर्धन हेतु), के तहत जारी नियमावली का तीखा विरोध हुआ। तथाकथित उच्च जातियों के नौजवान ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जैसे उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। हालांकि विरोध करने वाले संख्या में कम थे लेकिन उनके विरोध का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। इसका कारण यह है कि शक्ति के केंद्र में उनकी पहुँच ज्यादा है। नीति-निर्धारण करने वाले स्थानों पर बैठे लोग उनके साथ ही खड़े होते हैं। केवल यही तथ्य कि कम लोगो के विरोध का अधिक प्रभाव और असर हुआ है, UGC द्वारा जारी नई नियमावली की सार्थकता और ज़रूरत को न्यायोचित ठहराता है। यह देश में विद्यमान अमानवीय जाति प्रथा का परिणाम है।

*समानता से घबराहट: असुरक्षा नहीं, श्रेष्ठता पर चोट*
कितना विचित्र है कि यह विरोध एक ऐसे प्रयास का हो रहा है, जिसका मकसद ही भेदभाव को रोकना है। हालांकि यह समझना ज्यादा जरुरी है कि यह कदम भी बहुत ढीला ढाला और अनमना है। लेकिन फिर भी इतना घोर विरोध? क्या समानता के लिए प्रयास करना हमारे समाज में इतना बुरा हो गया है। यह पूरा प्रकरण दरअसल उच्च जातियों की असुरक्षा का मसला ही नहीं है। इसका तो केवल हवाला देकर आन्दोलित, यूं कहें तो आक्रोशित किया गया है नौजवानों को। असल कारण तो है जाति श्रेष्ठता को मिल रही चुनौती को ख़ारिज करना। डर यह नहीं है कि इस नियमावली के तहत गलत शिकायतें दर्ज होंगी, लेकिन डर यह था कि शिकायतें दर्ज होंगी। शिकायतें दर्ज होंगी समानता को जार-जार करने वाले मनुवादी विचार के वाहकों के खिलाफ, जो इंसानों में भेदभाव करना अपना हक़ समझते है। चिंता तो असल यह थी कि समानता का पाठ पढ़ाने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में खुले में चल रहे सर्वमान्य भेदभाव और गैर-बराबरी के खिलाफ कमजोर ही सही, आवाज उठाने की कुछ ताकत यह नियमावली देती है।
हालांकि अगर इस पूरे विरोध अभियान की भाषा और शैली को देखे तो साफ हो जाता है कि देश में राजनीतिक तौर पर मनुवाद कितना हावी हो गया है। विरोध करने वाले बड़ी ही आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करे रहे थे और खुले तौर पर जातिसूचक शब्दावली का प्रयोग कर रहे थे। मीडिया की कवरेज भी जातीय समझ से ग्रसित और पूरी तरह एकपक्षीय थी। ऐसा दिखाया जा रहा था मानो इस नियमावली से हिन्दू समाज विभाजित हो जाएगा और जैसे इससे अगड़ी जातियों के लोग बेचारे बन जाएंगे। पूर्वाग्रह से ग्रसित मीडिया ने तो यह तक घोषित कर दिया कि इस नियमावली का दुरुपयोग ही होगा। एक चैनल के एंकर ने एक पैनलिस्ट से यहाँ तक कह दिया कि यदि मैं कुछ सवाल पूछ लूँ, तो कहीं आप मुझ पर एससी/एसटी एक्ट न लगा दें। जब उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगाई, तो कई चैनलों ने इसे पंडितों और क्षत्रियों की जीत घोषित किया और कहा कि यह देश को बाँटने वालों की हार है।

*यूजीसी नियमावली की संरचना : क्या है प्रस्ताव और उसका उद्देश्य?*
अभी तक यूजीसी की नियमावली पर खूब चर्चा हो चुकी है। 15 जनवरी से लागू की गई (जिस पर अब उच्चतम न्यायलय ने रोक लगा दी है) इस नियमावली के अनुसार प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को समान अवसर केंद्र का गठन करना अनिवार्य किया गया है, जिसका मकसद सब के लिए सामान अवसर उपलब्ध करवाना है। इस केंद्र के कार्य संचालन का प्रबंधन करने तथा भेदभाव से संबंधित शिकायतों की जाँच करने के लिए एक समानता समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी संरचना इस प्रकार होगी : शिक्षण संस्थान के प्रमुख इसके पदेन अध्यक्ष होंगे ; उच्च शिक्षा संस्थान के तीन प्रोफेसर/वरिष्ठ संकाय सदस्य इसके सदस्य होंगे ; एक गैर शिक्षण कर्मचारी सदस्य होगा ; प्रासंगिक अनुभव वाले नागरिक समाज के दो प्रतिनिधि सदस्य होंगे ; शैक्षणिक योग्यता/खेल उपलब्धि/सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर नामित किए जाने वाले दो छात्र प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ; तथा समान अवसर केंद्र के समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे, और समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से होगा।
योग्यता/खेल उपलब्धि/सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर नामित किए जाने वाले दो छात्र प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ; तथा समान अवसर केंद्र के समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे, और समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से होगा।
यह समिति वर्ष में दो बार अपनी बैठक करेगी और प्रत्येक छह माह में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी, जिसमें जाति-आधारित ड्रॉपआउट (बीच में पढ़ाई छोड़ने) की दर, प्राप्त कुल शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण शामिल होगा ; साथ ही 24 घंटे कार्यरत एक हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, प्रत्येक छात्रावास और विभाग में इक्विटी स्क्वाड का गठन किया जाएगा तथा इक्विटी एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे, जिनका दायित्व त्वरित हस्तक्षेप करना और जागरूकता फैलाना होगा ; किसी भी शिकायत के प्राप्त होते ही 24 घंटे के भीतर समिति की बैठक बुलाना अनिवार्य होगा और उस पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यवाही करनी होगी ; कार्यवाही की पर्याप्तता या अपर्याप्तता के संबंध में अपील के लिए एक निष्पक्ष लोकपाल (ओम्बुड्समैन) की व्यवस्था होगी)

*नियमावली की सीमाएँ और गंभीर खामियां*
हालांकि इस गाइडलाइन्स में कई कमियां है, जैसे यह भेदभाव की कोई साफ़ और पूरी परिभाषा नहीं देते हैं। इनमें ज़्यादा ज़ोर सिर्फ़ यह दिखाने पर है कि भेदभाव नहीं है, जबकि उच्च शिक्षा संस्थानों में मौजूद असली और रोज़मर्रा के भेदभाव के अनुभवों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। ज़रूरी है कि इस ढाँचे को और मज़बूत बनाया जाए, ताकि छात्रों और शिक्षकों को जिन-जिन तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उन्हें साफ़ तौर पर माना जाए, समझाया जाए, पहचाना जाए और उन्हें खत्म किया जा सके। एक बड़ी कमजोरी यह है कि समानता समिति (इक्विटी कमेटी) का गठन किसी संस्थान प्रमुख की इच्छा और मनमर्जी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि उसकी विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह गाइडलाइन्स केवल विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों तक ही सीमित हैं और आईआईटी, आईआईएम, एम्स तथा ऐसे अन्य केंद्रीय संस्थानों पर लागू नहीं होते, जो एक गंभीर कमी है ; सरकार को इस खामी को दूर करते हुए इन संस्थानों तक भी प्रभावी समानता तंत्र का विस्तार करना चाहिए। यूजीसी ने समानता समिति के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों के निपटारे के लिए ओम्बड्सपर्सन नियुक्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिया है, जबकि चूँकि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों के तहत स्थापित हैं, इसलिए संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों के अनुरूप ओम्बड्सपर्सन की नियुक्ति का अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के पास होना चाहिए।

*आंदोलनों की विरासत*
लेकिन इसके बावजूद एक लम्बे आंदोलन के बाद इस पड़ाव पर पहुंचना महत्वपूर्ण है। यह नियमावली कोई सरकार की वंचित तबकों की शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में उनकी बदतर हालत की कोई चिंता से नहीं उपजी है, बल्कि पिछले एक दशक में श्रेष्टता पर आधारित मनुवादी वैचारिकी वाली भाजपा सरकार का शासन वंचित समुदायों, विशेष तौर पर दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यंकों के खिलाफ हिंसक वातावरण पैदा करने वाला ही रहा है। इस नियमावली को लाने के पीछे आंदोलनों का एक लम्बा इतिहास रहा है, जो शुरू हुआ था हैदराबाद विश्वविद्यालय के रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या के खिलाफ न्याय के लिए शुरू हुए आंदोलन से। उस समय पूरे देश का छात्र समुदाय सडकों पर उतर आया था। लेकिन ऐसी घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस बीच 26 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर पायल तड़वी ने 2019 में मुंबई के बीवाईएल नायर अस्पताल में जातिगत भेदभाव और वरिष्ठ सहकर्मियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। हालाँकि वर्ष 2012 में यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव दिशा-निर्देश जारी किये थे, लेकिन रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी की दुखद मौतों से यह साबित होता है कि 2012 की यूजीसी दिशानिर्देश वास्तव में कितने खोखले और अप्रभावी थे। साथ ही यह मौतें देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जड़ जमाए जातिगत उत्पीड़न की सच्चाई को निर्ममता से उजागर करते है।
रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताएं (क्रमशः राधिका वेमुला और आबेदा सलीम तड़वी) इस आन्दोलन को अदालत में ले गई और 2019 में एक जनहित याचिका दायर की। इस जनहित याचिका में परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी तंत्र की मांग की गई थी। इस याचिका के तहत मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि यूजीसी ने याचिका में उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रारूप विनियम तैयार कर लिए हैं।

अप्रैल में अदालत ने स्पष्ट किया कि यूजीसी प्रारूप विनियमों को अंतिम रूप देकर अधिसूचित कर सकती है। अंतता सितंबर महीने में अदालत ने यूजीसी को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने और विनियमों की अधिसूचना के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया। इस प्रक्रिया का ही परिणाम है ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस’।
*बराबरी बनाम विभाजन : असली सवाल क्या है?*
अब यह देखना बहुत रोचक है कि जब न्याय के लिए कानूनी लड़ाई के बाद न्यायालय के हस्तक्षेप से ही यह नियमावली बनी और अदालत ने इसके महत्व पर टिप्पणी भी की, फिर उच्चतम न्यायालय ने ही इस पर रोक लगा दी। न केवल अस्थाई रोक लगा दी, बल्कि त्वरित सुनवाई भी की। उतना ही खेदजनक है न्यायालय की टिप्पणी। इस पर रोक लगाते हुए सीजेआई ने इन नियमों को ‘समाज को बांटने वाला’ और ‘पीछे ले जाने वाला’ बताया। प्रश्न तो यह है कि न्यायालय किस समाज को बांटने की बात कर रहा है, जो पहले से जातियों में न केवल बंटा है, बल्कि अन्यायपूर्ण तरीके से श्रेणीकृत भी है, जहां तथाकथित अगड़ी जातियां दलितों और आदिवासियों को प्रतिदिन उनकी दोयम स्थिति का आभास करवाती है।

यह केवल सच्चाई से आँखें मूंदने का मामला नहीं है, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था में व्याप्त जाति का भी परिचायक है। हमारी अदालतों में अक्सर जाति का मजाक बनाया जाता है और न्याय व्यवस्था में विद्यमान जाति-आधारित भेदभाव के कई प्रमाण उपलब्ध हैं। यहां केवल दो उदाहरण काफी है। 2001 में एक 30-सदस्यीय संसदीय समिति और 2014 में अनुसूचित जाति आयोग ने अपनी-अपनी रिपोर्टों में यह पुष्टि की कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भारतीय न्यायाधीशों में जातिगत पूर्वाग्रह मौजूद हैं, जो केवल उनकी सोच तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके न्यायिक फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। इन दोनों रिपोर्टों में न्यायिक व्यवस्था के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ विभिन्न प्रकार के जातिगत भेदभाव को दर्ज किया गया था, जबकि अक्टूबर 2021 में अमेरिकन बार एसोसिएशन के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट ने दलित वकीलों के साथ हो रहे अप्रत्यक्ष भेदभाव को रेखांकित किया, जिसमें उन्हें अच्छे ऑफिस न दिए जाना, सीनियर काउंसिल द्वारा कम वेतन देना, कार्यस्थल पर बुलिंग करना या उनसे निम्न स्तर के काम करवाना जैसे व्यवहार शामिल हैं।
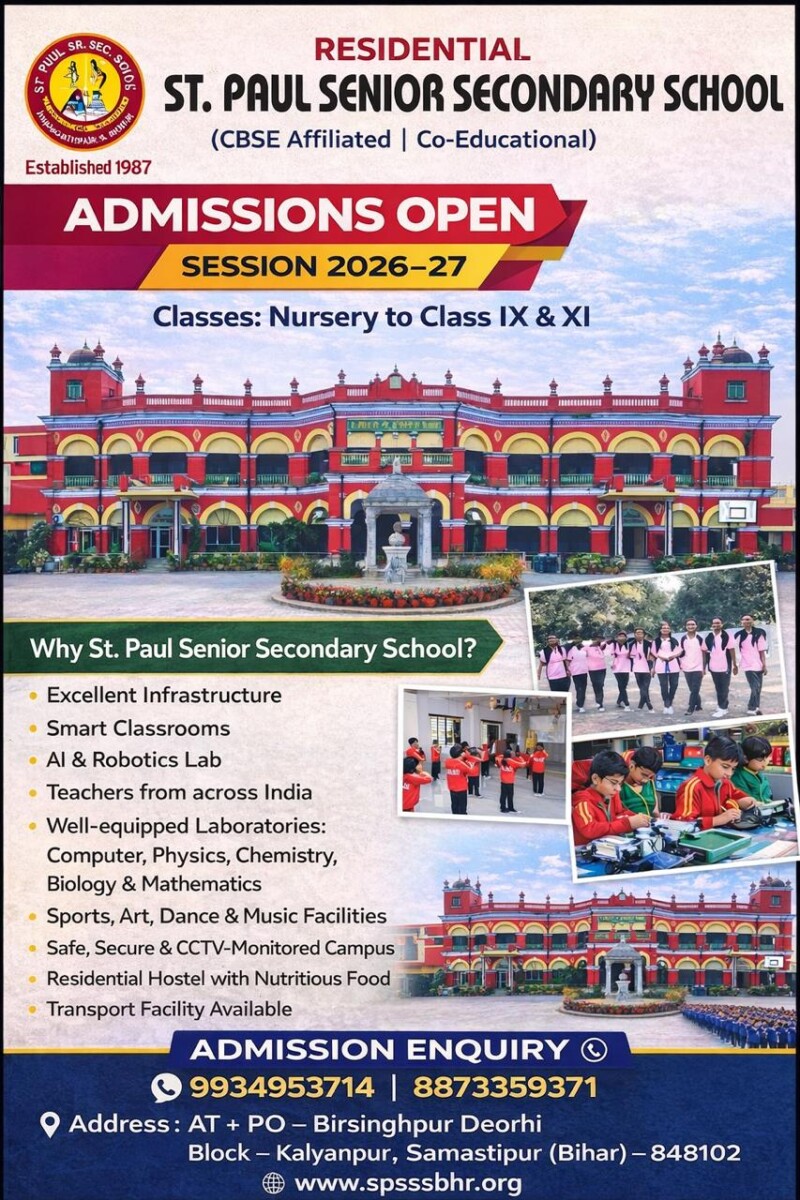
जब अदालतें भी जातीय उत्पीड़न से नहीं बची हैं, तो हमारे माननीय किस समाज को बाँटने की बात कर रहे है? यह एक नया तरीका है कि भेदभाव को अस्वीकार ही कर दो। यही तो आधार है पूरे देश में इस नियमावली के विरोध का। अगर समाज को बराबरी पर लाना है और एकता स्थापित करनी है, तो पहले से व्याप्त असमानता को स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ लड़ने के उपाय करने होंगे। यह महत्वपूर्ण पक्ष हमारे संविधान ने स्वीकार किया था और उसके अनुसार ही उपाय भी सुझाये थे।
*आँकड़े आईना दिखाते हैं*
गौरतलब है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में लगातार बढ़ रहे अत्याचार के मामले अदालत के रुख को आईना दिखाते है। यूजीसी द्वारा संसदीय समिति और सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति-आधारित भेदभाव की शिकायतों में पिछले पाँच वर्षों में 118.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के आंकड़े यह भी पुष्टि करते हैं कि जातिगत भेदभाव की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही संकाय सदस्यों में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है, जहां अनुसूचित जाति का नामांकन 14 प्रतिशत से घटकर केवल 6 प्रतिशत रह गया है, जो संस्थागत स्तर पर बढ़ते बहिष्करण की ओर इशारा करता है।
देश की राजधानी दिल्ली स्थित डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय में जाति के आधार पर हो रही रैगिंग के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले छात्र संघ के सदस्यों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर से निष्कासित कर दिया। यह वही छात्र संघ है, जिसे छात्रों ने लोकतांत्रिक तरीके से ठीक इसी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए चुना था। इन छात्रों का तथाकथित ‘अपराध’ सिर्फ़ इतना था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दलित छात्रों के खिलाफ उनकी जाति के आधार पर हो रही रैगिंग का विरोध किया और प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लेकिन प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय छात्र संघ के सदस्यों को ही दंडित कर दिया।
*मनुवादी वर्चस्व और राज्य सत्ता का गठजोड़*
विरोध करने वाले लोग एक बेहद बेढंगे और भ्रामक तर्क के साथ यह कह रहे थे कि उनकी जाति का नाम उन समूहों में शामिल नहीं है, जिनके खिलाफ भेदभाव हो सकता है। वे चाहते हैं कि इस नियमावली में उन जातियों और समूहों को भी शामिल किया जाए, जो भेदभाव के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह तर्क दरअसल देश में मौजूद जाति व्यवस्था और उसके गहरे सामाजिक प्रभावों को नकारने की एक कोशिश है। यह सवाल ठीक वैसा ही है, जैसे यह पूछा जाए कि महिला उत्पीड़न रोकने के लिए बने वुमन सेल में पुरुषों को क्यों शामिल नहीं किया गया। वजह बिल्कुल साफ़ है, जातिगत उत्पीड़न की संरचना ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ निर्मित हुई है। इसे स्वीकार करना किसी का बहिष्कार नहीं, बल्कि उस असमान यथार्थ को मान्यता देना है, जिसे सदियों से ‘सामान्य’ बनाकर स्वीकार किया जाता रहा है।
दूसरी बड़ी हाय-तौबा मचाई जा रही है कि इसका तथाकथित दुरूपयोग होने की संभावना पर। यह पहली बार नहीं है। जब भी समाज में भेदभाव को रोकने के लिए कोई प्रावधान लाया जाता है, तो भेदभाव करने वाले लोग तुरंत इसके दुरूपयोग की बात करने लगते हैं। यही तर्क और प्रचार हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लेकर भी देखा है। यह नियम किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को चुनौती देता है, जिसने जातिगत असमानता को अब तक ‘नॉर्मल’ बना रखा था। कैंपस में समता भाषणों से नहीं, बल्कि सख़्त, जवाबदेह और लागू होने वाले नियमों से आएगी।
हमारे अनुभव भी है कि कैसे हमारा समाज इस असरदार कानून को भी अपने जातीय प्रभाव से बेअसर कर देता है। हमने देखा है, मुक़दमा दर्ज होने के बाद भी न्याय लगभग असंभव हो जाता है वंचित तबकों के लिए। उल्टा अदालत की कार्यवाही पीड़ित के लिए ही दंड बन जाती है और आरोपी छूट जाते है। हाथरस गैंग रेप केस इसका सबसे जीता-जागता उदाहरण है। फिर कम दोषसिद्धि दर होने का हवाला देकर इस कानून के दुरूपयोग की बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया।
आज के समय में तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को संसद में पास करवाना संभव नहीं होता। इसके खिलाफ सरकार की सुरक्षा में देश की दमनकारियों व वर्चस्व वाली जातियों की मज़बूत लामबंदी हो जाती, जैसा कि यूजीसी की गाइडलाइन्स के बारे में हुआ है। यह अपने आप नहीं हुआ है, बल्कि यह आरएसएस के नेतृत्व में भाजपा के शासन का एक परिणाम है। यह आरएसएस के मनुवादी एजेंडे का मजबूत होना है।
*न्याय और समानता के लिए निर्णायक संघर्ष की ज़रूरत*
यूजीसी की यह नियमावली किसी समाज को बाँटने का औज़ार नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक अन्याय को चुनौती देने का प्रयास है, जिसे सदियों से ‘सामान्य’ बनाकर स्वीकार कर लिया गया है। बराबरी की बात करना अगर आज भी ‘विभाजन’ कहलाता है, तो यह हमारे लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और सामाजिक चेतना पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। जाति-आधारित उत्पीड़न को नकारना, उसके खिलाफ बने न्यूनतम संरक्षणों को भी ख़तरा बताना और हर प्रयास को ‘दुरुपयोग’ के भय से खारिज कर देना, असल में उसी मनुवादी व्यवस्था की रक्षा है, जो असमानता से पोषित होती है। अनगिनत नामहीन पीड़ितों की स्मृतियाँ हमसे यह सवाल करती हैं कि क्या हम बराबरी को सिर्फ़ संवैधानिक शब्दों में सीमित रखेंगे या उसे संस्थानों की ज़मीन पर उतारने का साहस भी करेंगे। अगर सचमुच एक समतामूलक, लोकतांत्रिक और एकजुट समाज बनाना है, तो पहले यह स्वीकार करना होगा कि समाज पहले से बँटा हुआ है और उसे जोड़ने का रास्ता केवल न्याय, जवाबदेही और समानता से होकर ही जाता है। इसलिए न्यायालय को उपरोक्त नियमावली में मौजूद कमियों के दूर कर, ज्यादा मज़बूत और प्रभावशाली गाइडलाइन्स लागू करनी चाहिए। देश के प्रगतिशील जनता के सामने भी यह ठोस सवाल है कि मनुवादी सोच की जीत होगी या सभी तरह भेदभाव को ख़त्म कर समतामूलक सोच को लागू करने के लिए देश निर्णायक लड़ाई में आगे बढ़ेगा।
(लेखक एसएफआई के पूर्व महासचिव और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त सचिव हैं। संपर्क : 9418484418)*



