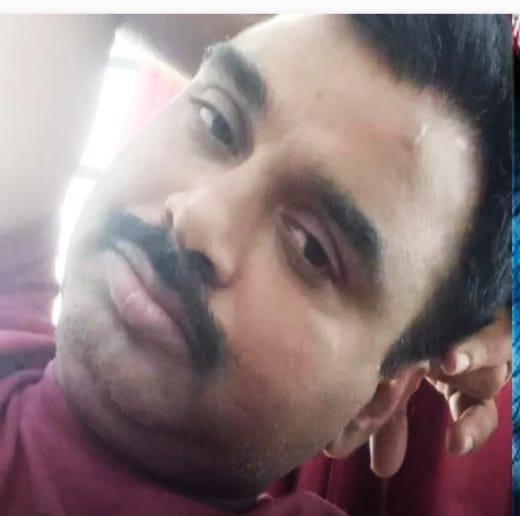डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और बौद्ध धर्म: समता, करुणा और सामाजिक पुनर्जागरण का मार्ग
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और बौद्ध धर्म: समता, करुणा और सामाजिक पुनर्जागरण का मार्ग  जे टी न्यूज, अररिया: भारतीय इतिहास के आधुनिक युग में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वह विराट व्यक्तित्व हैं जिन्होंने न केवल भारत के संविधान की रचना की, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और समता की क्रांतिकारी चेतना को साकार रूप दिया। उनका संपूर्ण जीवन एक महामानव की उस यात्रा का प्रतीक है जो शोषण, अपमान और असमानता से लड़ते हुए सम्यक जीवन मूल्यों की स्थापना करता है। इस संघर्षशील यात्रा का अंतिम पड़ाव था — बौद्ध धर्म की ओर लौटना।
जे टी न्यूज, अररिया: भारतीय इतिहास के आधुनिक युग में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वह विराट व्यक्तित्व हैं जिन्होंने न केवल भारत के संविधान की रचना की, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और समता की क्रांतिकारी चेतना को साकार रूप दिया। उनका संपूर्ण जीवन एक महामानव की उस यात्रा का प्रतीक है जो शोषण, अपमान और असमानता से लड़ते हुए सम्यक जीवन मूल्यों की स्थापना करता है। इस संघर्षशील यात्रा का अंतिम पड़ाव था — बौद्ध धर्म की ओर लौटना।
धर्म की पुनर्व्याख्या: आंबेडकर का दृष्टिकोण
डॉ. आंबेडकर के लिए धर्म कोई कर्मकांड या जन्म-आधारित व्यवस्था नहीं, बल्कि मानव-मुक्ति और आत्म-सम्मान की आधारभूमि थी। उन्होंने धर्म को आत्मा की मुक्ति के साथ-साथ समाज की मुक्ति का साधन माना। जाति प्रथा की बेड़ियों में जकड़े हिंदू धर्म ने जहाँ उन्हें अपमानित किया, वहीं बौद्ध धर्म में उन्होंने वह आत्मिक शांति, तर्कशीलता और समानता का आलोक पाया जिसकी उन्हें तलाश थी।बुद्ध का यह सन्देश कि – “न जात्या ब्राह्मणो होता, न जात्या होता शूद्रको” (ब्राह्मण या शूद्र कर्म से बनते हैं, जन्म से नहीं) — डॉ. आंबेडकर के विचारों का मूल आधार बन गया।  नवयान आंदोलन: आस्था से अधिक एक सामाजिक क्रांति 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की ऐतिहासिक भूमि पर डॉ. आंबेडकर ने पाँच लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर ‘नवयान’ आंदोलन की शुरुआत की। यह न केवल धार्मिक दीक्षा थी, बल्कि यह उस युगांतरकारी बदलाव का उद्घोष था जो भारत के दलित समाज को सामाजिक गुलामी से मुक्त करने की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम था। नवयान बौद्ध धर्म, मूलतः वही बुद्ध का धम्म था — परंतु आंबेडकर की सामाजिक दृष्टि और यथार्थवादी व्याख्या से सम्पन्न। यह धम्म अब केवल मोक्ष का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, समानता और सामाजिक न्याय का आंदोलन बन गया।
नवयान आंदोलन: आस्था से अधिक एक सामाजिक क्रांति 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की ऐतिहासिक भूमि पर डॉ. आंबेडकर ने पाँच लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर ‘नवयान’ आंदोलन की शुरुआत की। यह न केवल धार्मिक दीक्षा थी, बल्कि यह उस युगांतरकारी बदलाव का उद्घोष था जो भारत के दलित समाज को सामाजिक गुलामी से मुक्त करने की दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम था। नवयान बौद्ध धर्म, मूलतः वही बुद्ध का धम्म था — परंतु आंबेडकर की सामाजिक दृष्टि और यथार्थवादी व्याख्या से सम्पन्न। यह धम्म अब केवल मोक्ष का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, समानता और सामाजिक न्याय का आंदोलन बन गया।
बौद्ध धर्म: सम्यक जीवन की प्रेरणा
बौद्ध धर्म में वर्णित चार आर्य सत्य और आर्य अष्टांग मार्ग न केवल आध्यात्मिक उन्नति का, बल्कि नैतिक जीवन और सामाजिक समरसता का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। ये आठ अंग — सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, और सम्यक समाधि — डॉ. आंबेडकर के जीवन और उनके संविधान दर्शन के भी मूलतत्त्व हैं।
बौद्ध धर्म की अहिंसा, करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, शील और समता की शिक्षाएं आज भी सामाजिक नव निर्माण का आधार बन सकती हैं।
22 प्रतिज्ञाएं: पराधीनता से स्वतंत्रता की घोषणा
डॉ. आंबेडकर द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाएं महज धार्मिक संकल्प नहीं थीं, बल्कि यह जातिवादी व्यवस्था से पूर्णत: विच्छेद का साहसिक और वैचारिक उद्घोष थीं। उन्होंने न केवल ब्राह्मणवादी परंपराओं का त्याग किया, बल्कि अपने अनुयायियों को चेतना दी कि अब वे किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, वर्णव्यवस्था या असमानता को स्वीकार नहीं करेंगे।
बौद्ध धर्म और भारतीय संविधान: आंतरिक साम्यता
डॉ. आंबेडकर ने जिन मूल्यों पर भारतीय संविधान की नींव रखी — न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व — वे सभी बौद्ध धर्म के मूल विचारों से गहराई से जुड़े हैं। संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का धर्मग्रंथ बन गया। डॉ. आंबेडकर ने इसे एक ऐसा उपकरण बनाया, जो ‘धम्म’ के पथ पर चलते हुए भारत को समता और मानवता का राष्ट्र बना सके। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और बौद्ध धर्म एक-दूसरे के पूरक नहीं, बल्कि एक ही धम्म चेतना के दो अभिव्यक्त स्वरूप हैं। एक ने विचार दिया, दूसरे ने उसे सामाजिक रूपांतरण का आधार बनाया। डॉ. आंबेडकर का बौद्ध धर्म अंगीकार इतिहास की एक वैचारिक क्रांति थी, जिसने करोड़ों जीवनों को नया अर्थ, नई दिशा और नया स्वाभिमान दिया। आज जब विश्व शांति, सामाजिक समरसता और मानवीय अधिकारों की चर्चा होती है, तो डॉ. आंबेडकर और बुद्ध की साझा धारा उसमें सबसे उज्ज्वल प्रकाश की तरह उपस्थित होती है। वे केवल भारत के नहीं, समस्त मानवता के पथप्रदर्शक हैं। ऐसे युगपुरुष को कोटिशः नमन।
आज जब विश्व शांति, सामाजिक समरसता और मानवीय अधिकारों की चर्चा होती है, तो डॉ. आंबेडकर और बुद्ध की साझा धारा उसमें सबसे उज्ज्वल प्रकाश की तरह उपस्थित होती है। वे केवल भारत के नहीं, समस्त मानवता के पथप्रदर्शक हैं। ऐसे युगपुरुष को कोटिशः नमन।